भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2014 में अहमदाबाद की मुलाक़ात हो या 2019 में महाबलीपुरम में एक साथ सैर करना, तब दोनों देशों के बीच मधुर लगे रहे रिश्ते अब कड़वाहट और टकराव से भर गए हैं.
चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगी भावना हमेशा रही है लेकिन बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नज़र आ रही थी. लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच फिर से वही कड़वाहट पैदा कर दी है.
झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और चीन और भारत एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगा रहे हैं. इधर भारत में चीनी विरोध लहर चल पड़ी है और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही है.
ऐसे में चीन और भारत के रिश्ते जल्द ही फिर से पटरी पर आते मुश्किल लग रहे हैं. लोगों में भावनात्मक उफान है और सीमा पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जान देने वाले सैनिकों को नहीं भूला जाएगा.
इन हालात में चीन से बिगड़ते संबंधों के बीच भारत के पास संतुलन बनाने के लिए कौन से विकल्प हैं? भारत किस तरह दक्षिण एशिया में चीन का सामना करते हुए अपनी स्थिति मज़बूत कर सकता है.
रिश्ते सुधरने में लंबा समय लगेगा
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी अध्ययन केंद्र में प्रोफ़ेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का मानना है कि भारत-चीन के बीच रिश्ते ठीक होना बहुत मुश्किल लग रहा है. सैनिकों की मौत होने से दोनों के संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. विश्वास बहाली के प्रयास भी कमज़ोर हुए हैं.
वो कहते हैं, “चीन के ख़िलाफ़ बनी एक राष्ट्रीय धारणा का भी कारोबार पर असर पड़ेगा. चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है. ऐसे में संबंधों को सामान्य बना पाना आसान नहीं होता. हालाँकि, कूटनीति और कारोबार हमेशा चलते रहते हैं लेकिन बाहरी तौर पर गर्मजोशी नहीं रहती. कारोबारी निर्भरता बढ़ने से जो लोगों में संपर्क बढ़ा था और दूरी कम हुई थी, उसे वापस पाने में समय लगेगा.”
भारत और चीन आपसी सहयोगी भी हैं और प्रतियोगिता भी. ऐसे में अगर बिगड़ते संबंधों के साथ चीन भारत के लिए चुनौती बनकर आता है, तो भारत के लिए उसका सामना करने और संतुलन बनाने के लिए क्या विकल्प होंगे?
विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने भी बेहतर दिखें लेकिन एक आंतिरक दूरी और प्रतियोगिता बनी रहती है. दोनों देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं. इसलिए भारत एशिया में चीन के साथ संतुलन बनाने के लिए पहले से ही प्रयास करता है.
अब उसे अपने प्रयासों में तेज़ी लानी होगी. इसमें दो मुख्य तरीक़े हैं-भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी और पश्चिमी देशों से चीन की दूरी और भारत की नज़दीकी.
एक्ट ईस्ट पॉलिसी‘ पर फ़ोकस
भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में बदल दिया. इसके तहत भारत ने एशिया के दूसरे देशों में आर्थिक विकास के अवसर खोजने पर ज़ोर दिया.
लेकिन, आर्थिक फ़ोकस वाली भारत की ये नीति धीरे-धीरे कूटनीतिक हो गई. भारत दक्षिण पूर्वी देशों से कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाना चाहता है. मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2015 में एक अरब डॉलर की घोषणा भी की थी.
म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, जो भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे है. भारत, थाइलैंड और म्यांमार 1400 किमी. लंबे एक हाईवे पर काम कर रहे हैं.
दक्षिण एशियाई देशों जैसे थाइलैंड, वियतनाम, म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपिंस और कंबोडिया जैसे देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की इस नीति को चीन के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति के तौर पर भी देखा जाता है.
श्रीकांत कोंडापल्ली कहते हैं कि इस नीति में तीन चीजें हैं- कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन तीन ‘सी’ का ज़िक्र किया था. भारत को पहले इन देशों के साथ संबंध मज़बूत करके अपनी क्षमता बढ़ानी होगी. चीन के साथ संतुलन तभी बनेगा जब आप क्षमतावान होंगे.
एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत सरकार अपना आधारभूत ढांचा विकसित करने की कोशिश कर रही है, जैसे सड़कें और हाइवे बनाना. साथ ही कारोबार बढ़ाने पर भी सरकार का फ़ोकस है.
आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) देशों के साथ भारत निवेश बढ़ा रहा है. वहीं, संस्कृति की बात करें तो कुछ दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत की संस्कृति मिलती-जुलती है. इस सामनता को उभारकर देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाई जा रही है.
आसियान का उद्देश्य ही है कि सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को क़ायम रखा जाए. साथ ही झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा हो.
चीन के ख़राब संबंधों से कितना फ़ायदा?
भारत और चीन दोनों ही एक-दूसरे के पड़ोसियों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें करते रहे हैं. लेकिन, चीन ने जिस तरह विवादित क्षेत्रों में आक्रामक रुख़ अपनाया है, इससे उस क्षेत्र के देशों की चिंताएँ बढ़ी हैं और भारत को इससे अपना असर बढ़ाने में मदद मिली है. विशेषज्ञ भारत के लिए इसे एक मौक़ा मानते हैं.
दक्षिण चीन सागर के नटूना आइलैंड पर अधिकार को लेकर चीन का इंडोनेशिया के साथ सालों से विवाद चल रहा है. दक्षिण चीन सागर में ही पारसेल आइलैंड्स को लेकर चीन और वियतनाम आमने-सामने हैं.
दोनों देशों के बीच स्पार्टी आइलैंड्स को लेकर भी विवाद चल रहा है. दक्षिण चीन सागर में ही जेम्स शोल पर चीन और मलेशिया दोनों अपना दावा करते हैं.
चीन, दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है. इसके कारण आसपास के देशों के साथ इसका तनाव तो पहले से ही है. लेकिन अब अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून के तहत नौवहन का मुद्दा उठाकर चीन को चेतावनी दी है.
ये परिस्थितियाँ भारत के हक़ में कितनी जाती हैं इसे लेकर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च फेलो और चीन मामलों के जानकार अतुल भारद्वाज कहते हैं कि भारत अकेला ही चीन के साथ संतुलन नहीं बना सकता.
ऐसे में उसे दूसरे देशों का साथ मिलने से मदद मिल सकती है. इसे लेकर भारत को अपने प्रयास तेज़ करने होंगे.
वहीं श्रीकांत कोंडापल्ली का कहना है कि भारत इन देशों से संबंध बेहतर करके ना सिर्फ़ चीन की चिंताएँ बढ़ा सकता है बल्कि खुद को मजबूत भी कर सकता है.
उदाहरण के तौर पर भारत और जापान के बीच तीन-चार क्षेत्रों में टू प्लस टू वार्ता बढ़ाने की कोशिश की गई. जापान भारत को अर्थव्यवस्था और तकनीक के स्तर पर मदद कर रहा है. जैसे बुलेट ट्रेन और दिल्ली-मुंबई इनवेस्टमेंट कॉरिडोर के लिए जापान ने भारत को कर्ज दिया.
वो कहते हैं, ”इसी तरह जापान एक समुद्री ताक़त है जिससे भारत अपनी क्षमताएँ बढ़ा सकता है. तीसरा अंतरिक्ष में और चौथा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भारत और जापान सहयोग कर रहे हैं. अगर आप इन देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएँगे तो इससे बाज़ार और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी. इससे लोगों का संपर्क और परिवहन बढ़ जाता है.”



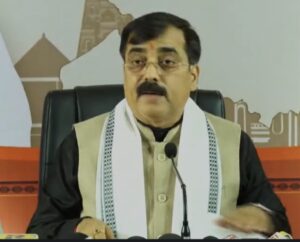


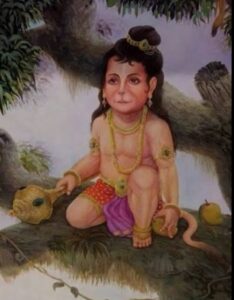


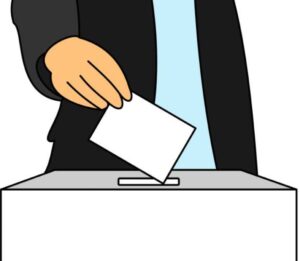


Be First to Comment